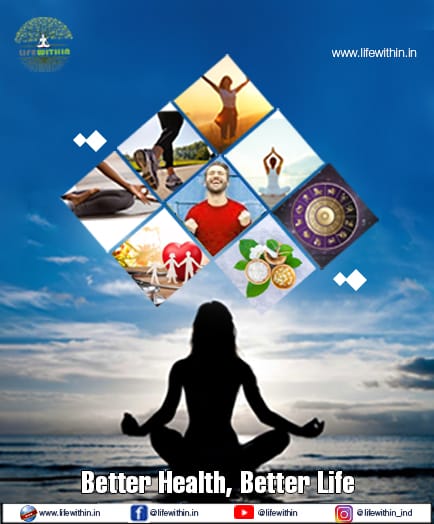Wellness Wonders: Become the Choreographer of your own Life | Dr. Mickey Mehta
- May 03, 2021
- 1382 View
Power of Gratitude: Scientifically Proven Benefits of Gratitude | Dr. Neeta Bheda
- May 03, 2021
- 1308 View
आदि-अनादि काल से हमारे संतों, शास्त्रों, गुरुओं और महापुरुषों ने हमें मार्ग की यात्रा और मंजिल का ज्ञान दिया, परन्तु हम...

मंजिल दूर नहीं, बस चलने की देरी है
आदि-अनादि काल से हमारे संतों, शास्त्रों, गुरुओं और महापुरुषों ने हमें मार्ग की यात्रा और मंजिल का ज्ञान दिया, परन्तु हम उस ज्ञान को न समझकर स्वार्थसिद्धि के चलते अपने हिसाब से चलने लगे। यात्रा और मार्ग ये उच्चकोटि के उच्च लोगों के लिए होते हैं। सामान्य लोगों के लिए शायद इन सबको समझ पाना असंभव सा प्रतीत होता है। एक महान संत की कही गई बात मौजूदा आलेख के संदर्भ में बिल्कुल प्रासांगिक प्रतीत होती है अतरू आपके समक्ष उसे रखना चाहूंगा। धर्म विचार में ही हो, तो उससे ज्यादा असत्य और कुछ भी नहीं है। धर्म शास्त्रों में ही है, इसलिए तो निष्क्रिय है। धर्म संप्रदायों में ही है, इसलिए तो धर्म धर्म ही नहीं है। धर्म तो जीवन में हो, तभी जीवित बनता है और सत्य बनता है। जहां सत्य है, वहां शक्ति है, वहां गति है। जहां गति है, वहां जीवन है।
आलेख के शीर्षक का भावार्थ है कि अपनी गलती को स्वीकार करना। जब तक हम अपनी गलतियों को गिनेंगे नहीं तो गलतियाँ बढ़ती ही जाएंगी। आज इस कलयुग में धर्म के विनाश का मूल कारण भी यही है। सामाजिक अपराधों में बेतहाशा बढ़ोत्तरी की भी प्रमुख वजह यही है। एक बहुरूपिए ने किसी सम्राट के द्वार पर जाकर कहा- पांच रुपए दान में चाहिए। सम्राट बोला- मैं कलाकर को पुरस्कार तो दे सकता हूं, लेकिन दान नहीं। बहुरूपिया मुस्कुराया और वापस लौट गया। लेकिन जाते-जाते कह गया महाराज, मैं भी दान ले सका तभी पुरस्कार लूंगा। बात आई और गई। कुछ दिनों के बाद राजधानी में एक अद्भूत साधु के आगमन की खबर विद्युत की भांति फैली। नगर के बाहर एक युवा साधु समाधि मुद्रा में बैठा था। न तो कुछ बोलता था, न आंखे ही खोलता था, और न हिलता-डुलता था। लोगों के झुंड के झुंड उसके दर्शन को पहुंच रहे थे। मेवा-मिष्ठान के ढेर उसके पास लग गए थे, लेकिन वह तो समाधि में था और उसे कुछ भी पता नहीं था। एक दिन बीत गया। दूसरा दिन भी बीत गया भीड़ रोज बढ़ती ही जाती थी। तीसरे दिन सुबह स्वयं सम्राट भी साधु के दर्शन को गए। उन्होंने एक लाख स्वर्ण मुद्राएं साधु के चरण में रख आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की। किंतु साधु तो पर्वत की भांति अचल थी। कोई भी प्रलोभन उसे डिगाने में असमर्थ था। चैथे दिन लोगों ने देखा कि रात्रि में साधु विलीन हो गया था। उस दिन सम्राट के दरबार में वह बहुरूपिया उपस्थित हुआ और बोला एक लाख स्वर्ण-मुद्राओं का दान तो आप मेरे सामने कर ही चुके है, अब मेरा पांच रुपए का पुरस्कार मुझे मिल जाए। सम्राट तो हैरान हो गया। उसने बहुरूपिए से कहा पागल तूने एक लाख स्वर्ण-मुद्राएं क्यों छोड़ी? और अब पांच रुपए मांग रहा है! बहुरूपिए ने कहा महाराज, जब आपने दान नहीं दिया था, तो मैं भी दान कैसे स्वीकार करता? बस अपने श्रम का पुरस्कार ही पर्याप्त है। फिर तब मैं साधु था। झूठा ही सही, तो भी साधु था, और साधु के वेश की लाज रखनी आवश्यक थी! इस कहानी पर विचार करने से बहुत सी बातें ख्याल में आती हैं। बहुरूपिए साधु हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि साधुओं के तथाकथित वेश में बहुरूपियों को सुविधा है। वेश जहां महत्वपूर्ण है, वहां सहज ही बहुरूपियों को सुविधा है। फिर वह बहुरूपिया तो साधु-चित्त था। इसलिए एक लाख स्वर्ण-मुद्राएं छोड़ कर पांच रुपए लेने को राजी हुआ। लेकिन सभी बहुरूपियों से इतने साधु-चित्त होने की आशा करनी उचित नहीं है। सम्राट धोखे में पड़ा, वेश के कारण। वेश धोखा दे सकता है। इसीलिए धोखा देने वालो ने वेश को प्रधान बना लिया है। और जब व्यक्ति दूसरों को धोखा देने में सफल हो जाता है, तो फिर वह सफलता स्वयं को भी धोखा देने का सुदृढ़ आधार बन जाती है। जब तक हम अंतर नहीं करेंगे तब तक हमारी यात्रा अंतकरण की तरफ नहीं चलेगी। अंतर हमें बिंदु और सिंधु के बीच में करना चाहिए, देव और महादेव, ईश्वर और महेश्वर तथा महेश्वर और परमेश्वर के बीच में करना चाहिए। अगर हम इस तरफ चलेंगे फिर मंजिल दूर नहीं, देरी बस चलने की है।